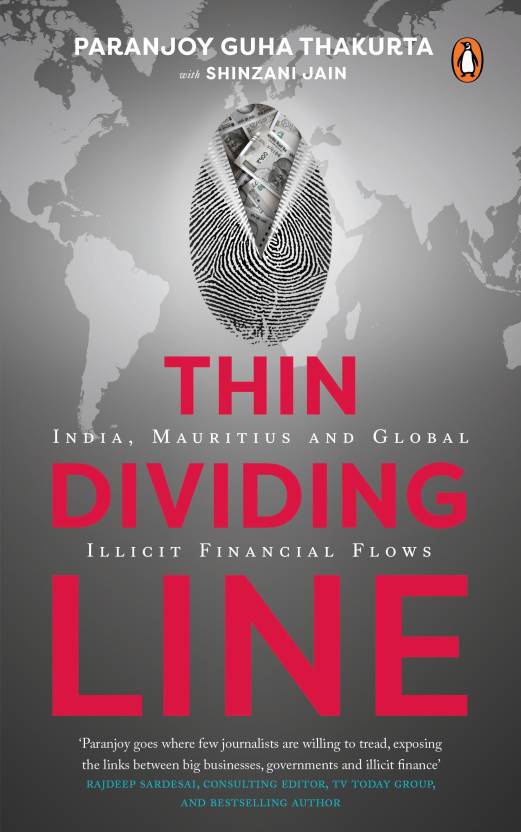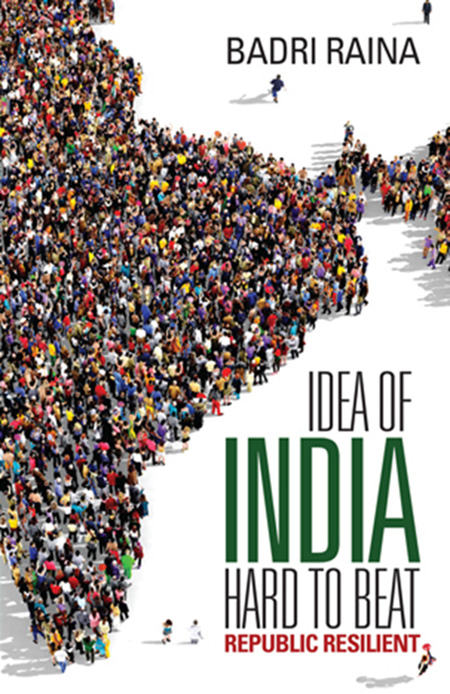भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार के अनेक वादे किए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन वादों को अमल में लाने में बहुत कम या कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। वास्तव में, पिछले एक दशक में सरकार के कई फैसलों ने देश में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति को और खराब कर दिया है।
इनमें नवंबर, 2016 की नोटबंदी और इसके अगले साल 2017 में जल्दबाजी में लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और मार्च, 2020 में आई कोविड-19 महामारी के दौरान बिना किसी तैयारी के लागू किया गया लॉकडाउन शामिल है, जिनके कारण करोड़ों लोगों को शहरों से गांवों की ओर पलायन करना पड़ा।
इससे किसी शायद ही एतराज हो कि युवाओं को रोजगार देना देश में सबसे बड़ी न सही सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। क्यों? क्योंकि भारत की लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या में आधे से ज्यादा लोग 28 साल से कम उम्र के हैं और लगभग दो तिहाई 36 वर्ष से कम उम्र के हैं।
गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) की एक रिपोर्ट के मुताबिक
Ad Slide 1Ad Slide 2
2022-23 में युवाओं में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 45.4% तक पहुँच गई थी। तबसे इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। 2011-12 से 2022-23 के बीच, देश के आधे से अधिक पुरुष और दो तिहाई से अधिक महिलाएं, “स्वरोजगार” की श्रेणी में थीं, जो दरअसल इस बात का संकेत है कि उन्हें कोई उचित नौकरी नहीं मिली। कई अर्थशास्त्री स्वरोजगार को रोजगार का सबसे खराब रूप मानते हैं।
स्वरोजगार को नहीं माना जाता रोजगार
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO),जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है, स्वरोजगार को रोजगार नहीं मानता। जबकि भारत सरकार का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) इसे रोजगार मानता है। जुलाई,2023 से जून, 2024 तक के लिए सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey (PLFS) के आँकड़ों के अनुसार, देश की कुल श्रमशक्ति में पांच वर्षों में स्वराजोगार की हिस्सेदारी 53 % से बढ़कर 58% से अधिक हो गई।
चूंकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति धीमी रही है और श्रम भागीदारी (LFPR) में गिरावट आई है, ILO की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 ने देश के संरचनात्मक परिवर्तन को “ठहराव” का शिकार बताया है। LFPR वह अनुपात है, जो कुल श्रमबल और कामकाजी उम्र 15 से 64 वर्ष की आबादी के बीच होता है। रोजगार न सृजित कर पाने की अक्षमता और असफलता पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन का एक अहम कारण है।
सरकार की बाज़ार समर्थक नीतियाँ और योजनाएं नौकरियाँ पैदा करने में विफल रही हैं, क्योंकि ये मुख्यतः संगठित क्षेत्र की निजी कंपनियों की “मर्ज़ी” पर निर्भर करती हैं, जो पहले मुनाफा देखती हैं, रोजगार नहीं। बल्कि, जब कम कर्मचारियों से टेक्नोलॉजी के ज़रिये उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, तो कंपनियाँ उसी विकल्प को चुनती हैं।
असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्यम—विशेषकर एमएसएमई (MSME) ने बड़े कॉर्पोरेट की तुलना में कहीं अधिक नौकरियाँ पैदा की हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इन पर नोटबंदी और जल्दबाज़ी में लागू किए गए जीएसटी ने जबरदस्त असर डाला है। 1 जुलाई, 2017 से शुरू हुए जीएसटी के नियमों में अब तक 900 से अधिक बार बदलाव हो चुके हैं।
इससे सबसे ज़्यादा नुक़सान “श्रम-प्रधान” एमएसएमई को हुआ है, जैसे वस्त्र, जूते-चप्पल, फर्नीचर और रसोई के उपकरण (जैसे प्रेशर कुकर) बनाने वाले छोटे उद्यम। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस के अनुसार, 2006 से 2021 के बीच 24 लाख छोटे उद्योग बंद हुए, जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 1.3 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए।
तीसरा बड़ा झटका था—24 मार्च 2020 को अचानक घोषित लॉकडाउन। जब महामारी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही थीं, भारत की अर्थव्यवस्था 5.8% घट गई (वैश्विक औसत 3.1% के मुकाबले)। परंपरागत रूप से भारत में लोग गाँवों से शहरों की ओर काम की तलाश में जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार यह ट्रेंड उल्टा हो गया—लाखों लोगों को शहरों से वापस गाँवों में जाना पड़ा।
unemployment in india:मनरेगा (MNREGA) के तहत खर्च की गई राशि हर साल बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात ये है कि जिस योजना की प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में संसद में आलोचना की थी और इसे कांग्रेस की “असफलता का प्रतीक” बताया था, उसी योजना को सरकार को लॉकडाउन के बाद मज़बूरी में स्वीकार करना पड़ा। यह योजना आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है, भले ही इसके क्रियान्वयन में देरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हों।
2024-25 के बजट में मनरेगा के लिए अब तक की सबसे अधिक राशि—₹86,000 करोड़—आवंटित की गई, जो 2023-24 के वास्तविक खर्च के बराबर है। 2022-23 में तो यह राशि ₹90,000 करोड़ से भी अधिक थी, क्योंकि उस वर्ष लॉकडाउन के कारण पलायन और भी अधिक हुआ था।
सरकारी अर्थशास्त्रियों का दावा है कि देश में रोजगार की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है और भारत “सबसे तेज़ी से बढ़ती” बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए नौकरियाँ आएंगी। लेकिन असल बात यह है कि आर्थिक विकास समान रूप से होना चाहिए, न कि केवल अमीरों के लिए। जबकि आज देश की एक-तिहाई आबादी ₹100 रोज़ से कम में गुज़ारा करती है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी समेत कई टीमों ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे असमान देश बन गया है—आय और संपत्ति के वितरण के मामले में।
कांग्रेस पार्टी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बेरोज़गारी संकट “घातक” बन चुका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच 15,851 लोगों ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की।
सौ रुपये से कम गुजारा
निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ज़रूरी है, लेकिन जब तक नए निवेश नहीं होंगे और लोगों की खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी (जो कि अभी 20 वर्षों के निचले स्तर पर है), तब तक नौकरियाँ अपने आप पैदा नहीं होंगी। युवाओं की शिक्षा का स्तर ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अब वे कृषि में काम नहीं करना चाहते—न ही वे बिना वेतन वाले पारिवारिक श्रमिक बनना चाहते हैं।
भारत की जिस जनसांख्यिकीय लाभांश की बात की जाती थी, वह अब दुःस्वप्न बनती जा रही है। सच कहें तो मोदी सरकार की यह मान्यता कि अंबानी-अडानी जैसे बड़े पूँजीपति नौकरियाँ पैदा करेंगे और युवा खुद-ब-खुद स्वरोजगार करेंगे—ग़लत साबित हुई है। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, भारत में बेरोज़गारी संकट पर मामूली असर भी नहीं पड़ेगा।
(परंजय गुहाठाकुरता, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और इसके जनसंचार माध्यमों के कामकाज का अध्ययन करते हैं। वे एक लेखक, प्रकाशक, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, संगीत वीडियो के निर्माता और शिक्षक भी हैं।)